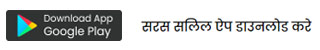हिन्दी अब पूरे मुल्क में पढ़ी-पढ़ाई जाएगी. यह अनिवार्य भाषा होगी. इसके अलावा दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरी भाषा क्षेत्रीय होगी. देशभर में ‘त्रिभाषा फार्मूला’ लागू होगा. केन्द्र सरकार की नयी शिक्षा नीति के तहत हिन्दी भाषा को पूरे देश में लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया नया ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया, देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया. विरोध के तीव्र स्वर खासतौर पर दक्षिण भारत से उठे. मजे की बात यह कि इस मामले में अपने ही मंत्रियों का विरोध भी प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा. हालत यह हो गयी कि लोग मरने-मारने तक की बातें करने लगे. द्रमुक के राज्यसभा सांसद तिरूचि सिवा ने तो केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया है कि हिन्दी को तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश कर केन्द्र-सरकार आग से खेलने का काम कर रही है. हिन्दी भाषा को तमिलनाडु पर थोपने की कोशिश को यहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम केन्द्र सरकार की ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए, किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं. वहीं, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी ट्वीट कर कहा कि तमिलों के खून में हिन्दी के लिए कोई जगह नहीं है. यह देश को बांटने वाला कदम होगा. यदि हमारे राज्य के लोगों पर इसे थोपने की कोशिश की गयी तो डीएमके इसे रोकने के लिए युद्ध करने को भी तैयार है. नये चुने गये सांसद लोकसभा में अपनी आवाज उठाएंगे. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, मक्कल नीधि मय्यम पार्टी के कमल हासन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया सब एकसुर में चीखे – हिन्दी हमारे माथे पर मत थोपो….
बवाल बढ़ा तो स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मोदी सरकार को यू-टर्न लेना पड़ा और ड्राफ्ट में बदलाव करते हुए हिन्दी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया. कहा जा रहा है कि अब संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को लचीला कर दिया गया है. अब इनमें किसी भी भाषा का जिक्र नहीं है. छात्रों को कोई भी तीन भाषा चुनने की स्वतंत्रता दे दी गयी है. सरकार को मामले की लीपापोती भी करनी पड़ी है. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सफाई देते हुए कहा, ‘सरकार अपनी नीति के तहत सभी भारतीय भाषाओं के विकास को प्रतिबद्ध है और किसी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. हमें नयी शिक्षा नीति का मसौदा प्राप्त हुआ है, यह सिर्फ रिपोर्ट है, फाइनल नीति नहीं है. इस पर लोगों एवं विभिन्न पक्षकारों की राय ली जाएगी, उसके बाद ही कुछ होगा. कहीं न कहीं लोगों को गलतफहमी हुई है.’
आखिर जिस मुद्दे पर आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक कभी पूरे देश में एकराय नहीं बनी, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी दिखा कर केन्द्र-सरकार को मुंह की तो खानी ही थी. सरकार की छीछालेदर हुई तो तमिलनाडु से सम्बन्ध रखने वाली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी मोर्चा संभालना पड़ा. गौरतलब है कि तमिलनाडु में मोदी-सरकार के फरमान का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, लिहाजा सीतारण ने ट्विटर कर कहा कि इस ड्राफ्ट को अमल में लाने से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी. जनता की राय सुनने के बाद ही ड्राफ्ट पॉलिसी लागू होगी. सभी भारतीय भाषाओं को पोषित करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ योजना लागू की थी. केन्द्र तमिल भाषा के सम्मान और विकास के लिए समर्थन देगा.’
ये भी पढ़ें- राजनीतिक रंजिशें किसी की सगी नहीं
वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी सरकार के बचाव में ट्वीट किया कि, ‘कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी. इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिए जाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाएगा. केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को सौंपी गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति महज एक मसौदा रिपोर्ट है. इस पर आम जनता से प्रतिक्रिया ली जाएगी. राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा. इसके बाद ही इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा. भारत सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है. कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी.’
हिन्दी थोपने और हिन्दी अपनाने में फर्क है
सर्वविदित है कि कोई चीज जबरन थोपा जाना किसी को पसन्द नहीं आता और न ही स्वीकार्य होता है. मगर ‘तानाशाही दिमाग’ इसको समझने में हमेशा नाकाम रहा है और हमेशा मुंह की खायी है. मोदी-सरकार भी इस रोग से अछूती नहीं है. सवाल यह कि हिन्दी की अनिवार्यता को लेकर बना नयी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट अगर अभी सिर्फ मसौदा था तो इस पर बिना विचार-विमर्श हुए और बिना परिणाम पर पहुंचे इसका ऐलान ही क्यों हुआ? राज्य सरकारों को तो छोड़िये, इसके लिए सरकार में मौजूद अपने ही मंत्रियों तक से विमर्श नहीं किया गया और देश भर के लिए हिन्दी को अनिवार्य बनाने की घोषणा कर दी गयी? क्या मोदी सरकार को लगता है कि उसने पूरे दमखम के साथ सरकार बना ली है, तो अब उसका हर फैसला सबको मानना ही पड़ेगा? या फिर प्रधानमंत्री पर भारत को ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का दबाव इतना ज्यादा है, कि अपने मंत्रियों और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने तक का वक्त उनको नहीं दिया जा रहा है?
दरअसल चाबुक के दम पर धर्म, जाति, भाषा, परिधान, आस्था, प्रेम जैसी चीजो में बदलाव या उसके लिए स्वीकार्यता पैदा नहीं की जा सकती है. थोपी हुई चीजें कभी दिल से स्वीकार्य नहीं होतीं, मगर यह सीधी सी बात दक्षिणपंथी विचारधारा में पगे लोगों की समझ में नहीं आती हैं. मोदी-सरकार को समझना चाहिए कि चीजें तब स्वीकार्य होती हैं, जब उनकी स्वीकार्यता के लिए माकूल वातावरण तैयार किया जाये, लोगों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हो, उस पर चर्चा हो, आलोचना हो, उसके प्रति आकर्षण पैदा किया जाये और उससे लोगों को कोई फायदा मिले.
हिन्दी के लिए किया क्या?
हिन्दी को शिक्षा में अनिवार्य भाषा बनाने के लिए उतावली मोदी-सरकार बताये अखिर बीते पांच साल के कार्यकाल में उसने हिन्दी के लिए क्या किया? देशभर में हिन्दी संस्थानों की हालत जर्जर है. हिन्दी के विद्वानों और लेखकों की कहीं कोई पूछ नहीं है. हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र बेरोजगारी का तमगा गले में डाल कर घूम रहे हैं. किसी प्राइवेट संस्थान में नौकरी के लिए जाते हैं तो उन्हें हिन्दीभाषी होने के कारण खुद पर शर्म आती है. देश भर में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है. किताबें अंग्रेजी में हैं. शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाते हैं. वे हिन्दी में बात करने वाले छात्रों को हेय दृष्टि से देखते हैं. उनके सवालों का समाधान करना तो दूर, सुनना तक नहीं चाहते. सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, जहां अंग्रेजी का ही बोलबाला है. चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का, बिजनेस का या वकालत का, कहां है हिन्दी?
सच पूछें तो आज हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाएं वे सौतेली बहनें हैं, जिनकी अम्मा अंग्रेजी है. अंग्रेजी में ही देश का राजकाज चलता है, कारोबार चलता है, विज्ञान चलता है, विश्वविद्यालय चलते हैं, मीडिया संस्थान और सारी बौद्धिकता चलती है. अंग्रेजी का विशेषाधिकार या आतंक इतना है कि अंग्रेजी बोल सकने वाला शख्स बिना किसी बहस के ही योग्य मान लिया जाता है. अंग्रेजी में कोई अप्रचलित शब्द आये तो आज भी लोग खुशी-खुशी डिक्शनरी पलटते हैं, जबकि हिन्दी का ऐसा कोई अप्रचलित शब्द अपनी भाषिक हैसियत की वजह से हंसी का पात्र बना दिया जाता है. पिछले तीन दशकों में हिन्दी की यह हैसियत और घटी है. सरकारी स्कूलों की बात छोड़ दें, तो पूरे देश में पढ़ाई-लिखाई की भाषा अंग्रेजी ही है. गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता है और हिन्दी घर में बोली जाने वाली एक बोली बन कर रह गयी है.
हां, यह कहा जा सकता है कि आज हिन्दी फिल्में विदेशों में खूब देखी जा रही हैं, हिन्दी सीरियल हर जगह देखे जा रहे हैं, कम्प्यूटर और स्मार्टफोन में हिन्दी को जगह मिल गयी है, इंटरनेट पर हिन्दी दिख रही है, मगर ऐसा कहने वाले यह नहीं देख रहे हैं कि यह हिन्दी बाजार की वजह से है, इसे सिर्फ बाजार ही बढ़ावा दे रहा है. यह सिर्फ एक बोली के रूप में इस्तेमाल हो रही है, जो बाजार कर रहा है. हिन्दी विशेषज्ञता की भाषा नहीं रह गयी है क्योंकि देश की सरकारों ने हिन्दी के हित में कभी कोई काम नहीं किया.
दूसरे, यह बात संघ और मोदी-सरकार को समझना चाहिए कि भाषा की विविधता ही इस देश की खूबसूरती है, भारत की पहचान है, उसकी समृद्धि है, उसका सौन्दर्य है और यह विविधता ही हम भारतीयों को एक-दूसरे के प्रति आकर्षण में बांधे रखने का काम भी करती है. हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, मगर उसके लिए वातावरण तैयार करना होगा ताकि उसकी सहज स्वीकार्यता बन सके. चाबुक के दम पर वह कभी स्वीकार्य नहीं होगी.
दक्षिण का हिन्दी से झगड़ा पुराना है
दक्षिण भारत ने तो अंग्रेजी पर ही निवेश किया है. उन्होंने अंग्रेजी का सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया है और तरक्की पायी है. सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दक्षिण भारत का योगदान अतुल्नीय है और यह अंग्रेजी के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता था. दूसरी ओर हिन्दी बोलने वाले लोग दक्षिण के राज्यों में खेतिहर मजदूर के रूप में काम करने के लिए जाते थे और आज भी जाते हैं. लिहाजा उनके द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी भाषा को तमिल लोग अपने सिर-माथे पर उठाएंगे, ऐसा सोचना भी मूर्खता है. साउथ में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव आज भी कमोबेश वैसा ही है, जैसा नेहरू या इंदिरा के वक्त में था. जवाहरलाल नेहरू ने भी हिन्दी को अनिवार्य बनाने की बहुत कोशिश की और हमेशा मुुंह की खायी. दरअसल जिस देश में हर दो कोस पर पानी और बानी बदलती हो, वहां एक भाषा को अनिवार्य करने का सपना पालना ही मूर्खता है.
ये भी पढ़ें- पौलिटिकल राउंडअप
गौरतलब है कि दक्षिण भारत से हिन्दी का झगड़ा बहुत पुराना है. हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भाषा को लेकर समझ साफ थी. वे इस बात को समझते थे कि अंग्रेजों की मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए भारतीय लोगों को अपनी भाषा बरतनी चाहिए. वे जानते थे कि हिन्दी में वो ताकत है कि वो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है और उस वक्त उसने बांधा भी, मगर वह इसलिए क्योंकि तब हम एक विदेशी ताकत से लड़ रहे थे. तब पूरे देश ने ‘हिन्दी’ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर उसके बाद इस हथियार को रख दिया गया. कहते हैं जब सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू ने हिन्दी को भारत में सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो उस वक्त ही तमिल नेताओं ने इसका घोर विरोध किया था. करीब नौ साल बाद सन् 1937 में तमिल नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास राज्य में हिन्दी लाने का समर्थन किया और हिन्दी को स्कूलों में अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया. अप्रैल 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी की 125 सैकेंडरी स्कूलों में हिन्दी को कम्पलसरी लैंग्वेज के तौर पर लागू भी कर दिया गया. मगर इसके खिलाफ आवाजें उठने लगीं. राजगोपालाचारी के इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा लिया तमिल शिक्षाविदों ने. उनका आरोप था कि सूबे की कांग्रेस सरकार हिन्दी के जरिए तमिल का गला घोंट रही है. इस आंदोलन के दौरान तमिल समर्थक उन स्कूलों के दरवाजे घेर कर बैठ गये, जहां हिन्दी पढ़ाये जाने का प्रस्ताव था. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार उन पर जबरन हिन्दी थोपना चाहती है. यह उनकी तमिल संस्कृति पर सीधा हमला है. 1 जून 1938 को सीवी राजगोपालाचारी के घर के सामने बड़ा प्रदर्शन हुआ. देखते ही देखते इस आंदोलन ने राजनीतिक मोड़ ले लिया. जो दो नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वे आगे आने वाले समय में तमिल अस्मिता आंदोलन का चेहरा बन गये. इसमें पहले थे ईवी रामास्वामी ‘पेरियार’ और दूसरे थे सीएन अन्ना दुरई, जिन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया था. द्रविड़ कषगम (डीके) की ओर से भी इसका घोर विरोध हुआ है और यह विरोध हिंसक झड़पों में बदल गया, जिसके चलते दो लोगों की मौत भी हुई. दो साल चले आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और हिन्दी को कम्पलसरी भाषा के तौर पर लागू करने का फैसला वापिस लेना पड़ा.
आजादी के वक्त भाषाओं के आधार पर राज्यों के विभाजन को लेकर कांग्रेस के भीतर आम सहमति बनी थी. महात्मा गांधी ने 10 अक्टूबर 1947 को अपने एक सहयोगी को लिखी चिट्ठी में कहा, ‘मेरा मानना है कि हमें भाषिक प्रांतों के निर्माण में जल्दी करनी चाहिए… कुछ समय के लिए यह भ्रम हो सकता है कि अलग-अलग भाषाएं अलग-अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन यह भी सम्भव है कि भाषिक आधार पर प्रदेशों के गठन के बाद यह गायब हो जाए.’ पं. जवाहर लाल नेहरू भी भारत की भाषिक विविधता को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन साम्प्रदायिक आधार पर हुए देश-विभाजन और मार-काट के बाद नेहरू और पटेल दोनों इस राय के हो चुके थे कि अब भाषिक आधार पर किसी विभाजन की जमीन तैयार न हो. मगर हिन्दी को वे तब भी किसी तरह देश की अनिवार्य भाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाये. दक्षिण भारत के तमाम प्रान्त इसका लगातार विरोध करते रहे. वे अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को ही ज्यादा महत्व देते रहे.
तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्ना दुरई द्वारा हिन्दी विरोध की कहानी तो बेहद जबरदस्त है. सन् 1960 में अन्ना दुरई ने अपने एक ख्यात भाषण में हिन्दी के संख्या बल के तर्क पर सवाल उठाया और कहा – शेरों के मुकाबले चूहों की संख्या ज्यादा है तो क्या चूहों को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए? उन्होंने मंच से हिन्दी को ललकारा और जनता से सवाल किया – मोर के मुकाबले कौवों की संख्या ज्यादा है तो क्या कौवों को राष्ट्रीय पक्षी बना देना चाहिए?
वर्ष 1965 में एक बार फिर दक्षिण भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई. मगर इस बार तो हिन्दी के खिलाफ स्थानीय लोगों का पारा बहुत ऊपर चढ़ गया. लोग खिलाफत के लिए सड़कों पर उतर आये और सरकार को काले झंडे दिखाये. पहले ये लोग 26 जनवरी को काले झंडे दिखाने वाले थे, मगर गणतन्त्र दिवस की लाज रखते हुए 25 जनवरी को यह काम किया गया. इस दिन को आज भी वहां ‘बलिदान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान हुई आगजनी और हिंसक झड़पों में सत्तर से ज्यादा लोगों की जानें गयी थीं. स्थानीय कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक हिंसक झड़प में आठ लोगों को जिन्दा जला दिया गया. डीएमके नेता डोराई मुरुगन को मद्रास शहर के पचाइअप्पन कॉलेज से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुर्इं. दो सप्ताह चले इस जबरदस्त विरोध को दबाने में सरकार के पसीने छूट गये.
हिन्दी के खिलाफ तमिलनाडु के मुखर विरोध की अभिव्यक्तियां बाद में महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में भी सुनायी देने लगीं. वे लोग मानते थे और आज भी मानते हैं कि उनके क्षेत्र में उनकी भाषा, हिन्दी के मुकाबले कहीं ज्यादा प्राचीन और समृद्ध है. पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी रॉय भी बांग्ला-भाषियों पर हिन्दी थोपे जाने के सख्त खिलाफ थे. दक्षिण भारत में हिन्दी के खिलाफ उठे इस तूफान को देखते हुए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी को राजभाषा अधिनियम में तुरंत संशोधन करना पड़ा था और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा देकर अमल में लाया गया था. यही नहीं, तमाम विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को जनता से क्षमायाचना तक करनी पड़ी थी और तमाम तरह के आश्वासन देने पड़े थे.
दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा
आजादी के इतने वर्ष बाद भी यदि हिन्दी दक्षिण भारतीयों का मन नहीं मोह पायी है, तो इसके दोषी केन्द्र सरकार ही नहीं, हिन्दी भाषी प्रदेश भी हैं. गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों में छात्रों ने तमिल, तेलुगू, मराठी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ी, मगर हिन्दी भाषी प्रदेशों में तेलुगू, तमिल, मराठी या बंगाली कोई नहीं पढ़ता, बल्कि यहां के छात्र अपनी तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत को अपनाते हैं, जो देश के किसी भी हिस्से में प्रमुखता से बोली नहीं जाती है. तो जब आप दक्षिण की भाषाओं के प्रति उपेक्षा बरतते हैं तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपकी भाषा को सिर-माथे पर लेगा? निस्संदेह संस्कृत एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, जिसका अलग से अध्ययन होना चाहिए, लेकिन इसे ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ में फिट कर हिन्दी भाषी प्रदेशों ने गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों से अपनी जो दूरी बढ़ायी, वह लगभग अक्षम्य है. आज अगर हिन्दी भाषी भी बड़ी तादाद में तमिल, तेलुगू, मराठी या बंगाली बोल रहे होते, तो बीते सत्तर सालों में हिन्दी का विरोध काफी कम हो चुका होता, लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे के करीब आ गये होते, मगर यह नहीं हुआ, सरकारों ने ऐसा होने नहीं दिया, इसलिए ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ के ताजा प्रस्ताव पर विरोध फिर से भड़क उठा है.
संघ के दबाव में मोदी
संघ के दबाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का सेहरा अपने सिर बांधने को उतावले हैं, इसीलिए पहले कदम के तौर पर हिन्दी को पूरे देश में अनिवार्य करने की तेजी दिखा दी, बगैर जमीनी हकीकत को समझे. वे नहीं जानते कि हिन्दू राष्ट्र की घोषणा करना तो बहुत आसान है, परंतु इसके पेंच बेहद खतरनाक हैं. मुख्य खतरा है कि यह कदम भारत को पाकिस्तान की तरह एक धर्मशासित देश में बदल देगा. यह हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करेगा, पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा, आंतरिक कलह और हिंसा का कारण बनेगा, भारत के सौन्दर्य को मिटा कर भारत की साख को नुकसान पहुंचाएगा. इससे भी अधिक क्षतिपूर्ण बात यह होगी कि एक हिन्दू राष्ट्र, भारत का विश्वगुरु के रूप में एक वैश्विक नेता बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म कर देगा. कोई भी सम्प्रभु देश विशुद्ध धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अलावा भारत के साथ न किसी संघ में शामिल होगा, न ही उसका अनुसरण करेगा. विडम्बना यह भी कि स्वयं हिन्दुत्व – जिसे इस कदम के समर्थक सबसे अधिक प्रदर्शित करना चाहते हैं, की भावना, परम्परा और प्रतिष्ठा को सबसे अधिक क्षति पहुंचाएगा.
ये भी पढ़ें- उंगली पर नीली स्याही से नहीं बदलेगी जिंदगी
उल्लेखनीय है कि साल 2008 तक नेपाल देश धरती का इकलौता हिन्दू राष्ट्र था. मगर वहां भी क्षत्रीय राजवंश का खात्मा हुआ और 2008 में नेपाल गणतंत्र बन गया. नेपाल को हिन्दू राष्ट्र भी सिर्फ इसलिए कहा जाता था क्योंकि हिन्दू संहिता मनुस्मृति के अनुसार कार्यकारी सत्ता का स्रोत राजा था. इसके अलावा वहां धार्मिक ग्रंथ की कोई और बात लागू नहीं थी क्योंकि ये ‘मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा’ के खिलाफ होती. बावजूद इसके नेपाल को अपनी हिन्दू राष्ट्र की छवि को तोड़ कर गणतन्त्र का रास्ता इख्तियार करना पड़ा.
हिन्दू राज के खिलाफ थे आंबेडकर
संविधान के रचयिता डॉ. आंबेडकर ने अपनी किताब ‘पाकिस्तान आॅर दि पार्टिशन आफ इण्डिया’ (1940) में चेताया है कि अगर हिन्दू राज हकीकत बनता है, तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा. हिन्दू कुछ भी कहें, हिन्दू धर्म स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता के लिए खतरा है. उस आधार पर वह लोकतन्त्र के साथ मेल नहीं खाता है. हिन्दू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए. डॉ. आंबेडकर ये बात बहुत साफतौर पर समझते थे कि हिन्दू राष्ट्र का सीधा अर्थ द्विज वर्चस्व की स्थापना था, यानी ब्राह्मण-वाद की स्थापना. वे हिन्दू राष्ट्र को मुसलमानों पर हिन्दुओं के वर्चस्व तक सीमित नहीं करते हैं, जैसा कि भारत का प्रगतिशील वामपंथी या उदारवादी लोग करते हैं. उनके लिए हिन्दू राष्ट्र का मतलब मुसलमानों के साथ दलित, ओबीसी और महिलाओं पर भी द्विजों यानी ब्राह्मणों के वर्चस्व की स्थापना था, जो एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश के लिए, जहां इतनी बोलियां, जातियां और भिन्न्ताएं हैं, कभी भी हितकारी नहीं है.
क्या है त्रिभाषा फार्मूला?
त्रिभाषा फॉर्मूला यानी बारहवीं कक्षा तक के सिलेबस में तीन भाषाओं को शामिल किया जाना. 1948 में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के आन्दोलन हो रहे थे. ठीक इसी समय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने पढ़ाई-लिखाई के लिए तीन भाषा का फॉर्मूला दिया था. इसके अनुसार अंग्रेजी, हिन्दी के अलावा एक स्थानीय भाषा भी पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने का प्रावधान किया गया. यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के सिलेबस को देखकर तैयार की गयी थी. वर्ष 1964 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में त्रिभाषा फॉर्मूले के लिए एक कमीशन बनाया गया. इस कमीशन ने 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंपी. वर्ष 1968 में भारतीय संसद ने कोठारी कमिशन की सिफारिश के आधार पर ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को स्वीकार कर लिया. उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अन्ना दुरई थे. अन्ना दुरई ने इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और तमिलनाडु की सरकारी स्कूलों से हिन्दी भाषा को हटा दिया.
दक्षिणी राज्यों के कड़े विरोध के चलते एजुकेशन पॉलिसी में ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को खारिज कर दिया गया. फिर साल 1990 में उर्दू के मशहूर लेखक अली सदर जाफरी के नेतृत्व में ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ पर विशेषज्ञों की एक कमिटी बनायी गयी. इस कमिटी ने अपनी सिफारिश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए अलग-अलग त्रिभाषा फॉर्मूले की सिफारिश की. इसके अनुसार उत्तर भारत में हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के तौर पर उर्दू को शामिल किया गया, वहीं दक्षिण भारत में हिन्दी और स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी को शामिल किये जाने की बात कही गयी. वर्ष 1992 में भारत की संसद ने इसको स्वीकार कर लिया. लेकिन गौरतलब बात यह है कि भरतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का विषय है. ऐसे में कोई भी राज्य ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है.
हिन्दी के विरोधी क्यों हैं तमिल
भारत गणराज्य में सैकड़ों भाषाएं हैं. ब्रिटिश राज के दौरान, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा थी. जब 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आयी, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न भाषाई समूहों को एकजुट करने के लिए हिन्दी को आम भाषा बनाने के प्रयास किये गये. 1918 की शुरुआत में, महात्मा गांधी ने ‘दक्षिण भारत प्रचार सभा’ (दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिए संस्थान) की स्थापना की. वर्ष 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कार्यवाही करने के लिए अंग्रेजी से हिन्दी की ओर रुख किया. महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों हिन्दी के समर्थक थे और कांग्रेस भारत के गैर-हिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी की शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी. लेकिन हिन्दी को आम भाषा बनाने का विचार दक्षिण के महान चिन्तक, विचारक और नेता ई.वी. रामासामी ‘पेरियार’ को कभी स्वीकार्य नहीं था. किसी भी किस्म की अंधश्रद्धा, कूपमंडूकता, जड़ता, अतार्किकता और विवेकहीनता पेरियार को स्वीकार नहीं थी. वर्चस्व, अन्याय, असमानता, पराधीनता और अज्ञानता के हर रूप को उन्होंने चुनौती दी. दक्षिण भारत में पेरियार को भगवान की तरह पूजा जाता है और उनके विचारों को बड़ा सम्मान प्राप्त है.
पेरियार ने दक्षिण में हिन्दी के प्रसार को तमिलों को उत्तर भारतीयों के अधीन एक प्रयास के रूप में देखा. उन्होंने कहा कि इस तरह ब्राह्मण तमिलों पर हिन्दी और संस्कृत थोपने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने इसके खिलाफ आन्दोलन किये, जिन्हें तमिलभाषी मुसलमानों का भी सहयोग मिला. पेरियार के हिन्दी विरोधी विचार के आधार में दरअसल हिन्दुओं का धर्मग्रन्थ रामायण था, जिसे पेरियार ने कभी धार्मिक किताब नहीं माना. उनका कहना था कि यह एक विशुद्ध राजनीतिक पुस्तक है; जिसे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा है. यह गैर-ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व को कायम करने वाला एक उपकरण मात्र है. उन्होंने कहा कि रामायण को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नजर में महान दिखें; महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके तथा उन्हें दासी बनाकर रखा जा सके. रामायण में जिस लड़ाई का वर्णन है, उसमें उत्तर का रहने वाला कोई भी (ब्राह्मण) या आर्य (देव) नहीं मारा गया. वे सारे लोग, जो इस युद्ध में मारे गये; वे तमिल थे. जिन्हें राक्षस कहा गया. रामायण की कथा का उद्देश्य तमिलों को नीचा दिखाना है. तमिलनाडु में इस कथा के प्रति सम्मान जताना तमिल समुदाय और देश के आत्मसम्मान के लिए खतरनाक और अपमानजनक है. उन्होंने कहा कि दक्षिण में हिन्दी का प्रसार ब्राह्मणों के धर्मग्रंथों, रूढ़ियों तथा ‘मनुस्मृति’ को तमिल समाज पर थोपना है; जो कि तमिलों के लिए अपमानजनक है.
हिन्दी की अनिवार्य शिक्षा को लेकर द्रविड़ आंदोलन का दशकों लम्बा विरोध ब्राह्मणवाद, संस्कृत के प्रभुत्व और हिन्दू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिये जाने के खिलाफ वैचारिक लड़ाई पर आधारित था. दक्षिण भारतीयों ने हमेशा संस्कृत को ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्मग्रंथों के प्रसार की सवारी के तौर पर ही देखा जो जातिगत एवं लैंगिक ऊंच-नीच की व्यवस्था को बनाये रखने का काम करती है. संस्कृत से नजदीकी को देखते हुए हिन्दी को भी जातिगत एवं लैंगिक शोषण की ‘पिछड़ी संस्कृति को बढ़ावा देनेवाली भाषा’ के तौर पर देखा गया.
ये भी पढ़ें- केजरीवाल को थप्पड़ मारने का मतलब
तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध इस आधार पर भी है कि आधुनिक, उपयोगी और प्रगतिशील ज्ञान यानी विज्ञान, तकनीक और तार्किक विचारों को हासिल करने की दृष्टि से हिन्दी समर्थ भाषा नहीं है. भले ही तमिलनाडु अपने कुशल श्रमबल के लिए पर्याप्त अच्छी नौकरियां पैदा कर पाने में समर्थ नहीं हो पाया है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा में निवेश ने उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवास को मुमकिन बनाया है. सर्वविदित है कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण ही भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियां कम लागत वाले प्रोग्रामिंग पेशेवरों की मौजूदगी का फायदा उठा पायीं और वैश्विक बाजार में अपने लिए जगह बना सकीं. यहां से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में गये हैं. भारत में आनेवाले धन (रेमिटेंसेज) के मामले में तमिलनाडु, केरल के बाद दूसरे स्थान पर आता है. राज्य की कुल आय में विदेशों से आनेवाले धन का योगदान 14 फीसदी है.
तमिलनाडु के लोगों की सोच के अनुसार हिन्दी उतनी पुरानी और समृद्ध भाषा नहीं है, जितनी तमिल और बांग्ला भाषाएं हैं. तमिल लोगों को यह भी लगता है कि हिन्दी की तुलना में अंग्रेजी समझना और सीखना ज्यादा आसान है. उनका कहना है कि आखिर वे अपने पास पहले से मौजूद एक आला दर्जे की भाषा को एक अविकसित और दोयम दर्जे की भाषा के लिए क्यों छोड़ दें?
Edited by – Neelesh Singh Sisodia