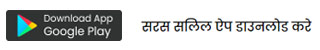हिन्दी अब पूरे मुल्क में पढ़ी-पढ़ाई जाएगी. यह अनिवार्य भाषा होगी. इसके अलावा दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरी भाषा क्षेत्रीय होगी. देशभर में ‘त्रिभाषा फार्मूला’ लागू होगा. केन्द्र सरकार की नयी शिक्षा नीति के तहत हिन्दी भाषा को पूरे देश में लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया नया ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया, देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया. विरोध के तीव्र स्वर खासतौर पर दक्षिण भारत से उठे. मजे की बात यह कि इस मामले में अपने ही मंत्रियों का विरोध भी प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा. हालत यह हो गयी कि लोग मरने-मारने तक की बातें करने लगे. द्रमुक के राज्यसभा सांसद तिरूचि सिवा ने तो केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया है कि हिन्दी को तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश कर केन्द्र-सरकार आग से खेलने का काम कर रही है. हिन्दी भाषा को तमिलनाडु पर थोपने की कोशिश को यहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम केन्द्र सरकार की ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए, किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं. वहीं, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी ट्वीट कर कहा कि तमिलों के खून में हिन्दी के लिए कोई जगह नहीं है. यह देश को बांटने वाला कदम होगा. यदि हमारे राज्य के लोगों पर इसे थोपने की कोशिश की गयी तो डीएमके इसे रोकने के लिए युद्ध करने को भी तैयार है. नये चुने गये सांसद लोकसभा में अपनी आवाज उठाएंगे. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, मक्कल नीधि मय्यम पार्टी के कमल हासन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया सब एकसुर में चीखे - हिन्दी हमारे माथे पर मत थोपो....
आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें
डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप
- 24 प्रिंट मैगजीन
डिजिटल
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप