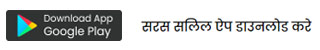संध्या हर साल दीवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ ही मनाती थी. वही शाम को पूजा-अर्चना, फिर घर-बाहर की दीया-बत्ती, पटाखे, खाना-पीना, पड़ोसियों-दोस्तों में मिठाईयों का आदान-प्रदान और बस लो मन गयी दीवाली. एक बारं संध्या कम्पनी के काम से लालपुर गयी थी. जिस औफिस में उसको काम था, उसके बगल वाली बिल्डिंग के लौन में उसने बहुत सारे नन्हें-नन्हें बच्चों को खेलते देखा था. पहले तो उसको लगा कि कोई छोटा-मोटा स्कूल है, मगर वहां लगे एक धुंधले से बोर्ड पर जब उसकी नजर पड़ी तो पता चला कि वह एक अनाथाश्रम है. लंच टाइम में फ्री होने पर संध्या उस अनाथाश्रम को देखने की इच्छा से भीतर चली गयी. दरअसल बच्चों के प्रति उसका खिचांव ही उसे वहां ले गया. बरसों से उसकी कोख सूनी थी. शादी के दस साल तक एक बच्चे की चाह में उसने शहर के हर डौक्टर, हर क्लीनिक के चक्कर लगा डाले थे, हर तरह की पूजा-पाठ कर ली थी, मगर उसकी मुराद पूरी नहीं हुई. धीरे-धीरे उसने अपना मन काम में लगा दिया और उसकी मां बनने की इच्छा कहीं भीतर दफन हो गयी. मगर उस दिन उन छोटे-छोटे बच्चों को लॉन में खेलता देख उसकी कामना फिर जाग उठी.
अनाथाश्रम में जीरो से सात सात तक के कोई पच्चीस बच्चे थे. बिन मां-बाप के बच्चे. जिन्हें पता ही नहीं कि परिवार क्या होता है. मां-बाप का प्यार क्या होता है. वे तो यहां बस आयाओं के रहमो-करम पर पल रहे थे. उनके इशारे पर उठते-बैठते, सोते-जागते और खेलते-खाते थे. संध्या ने देखा कि कुछ बच्चे यहां-वहां पड़े रो रहे थे, मगर उनको उठा कर छाती से चिपकाने वाला कोई नहीं था. आयाएं अपनी बातों में मशगूल थीं. संध्या ने अनाथाश्रम चलाने वाले के बारे में पूछा तो पता चला कि वह शनिवार को आते हैं और दोपहर तक रहते हैं. बाकी दिनों में अनाथाश्रम का सारा जिम्मा वहां काम करने वाली चार आयाएं ही उठाती थीं.
आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें
डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप
- 24 प्रिंट मैगजीन
डिजिटल
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप