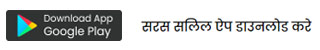नेपाल निर्वाचन आयोग ने संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है. चुनाव 26 नवंबर और सात दिसंबर को होने हैं. नई व्यवस्था के बाद प्रत्याशियों की अनुमानित संख्या को देखते हुए चुनावों पर अधिकतम दस अरब खर्च आना चाहिए, पर सच तो यह है कि शायद ही कोई इस सीमा का पालन करे, और उस हालत में यह खर्च 25-30 अरब तक पहुंच जाए, तो आश्चर्य न होगा.
दरअसल नेपाल के राजनीतिक दल अब मूलभूत सिद्धांतों से हटकर चुनाव के लिए धन जुटाने और बांटने पर केंद्रित होते गए हैं. उनकी इसी धनलिप्सा के कारण 1990 में लोकतंत्र बहाली के बाद इस बार के चुनाव पहली बार गैर-वैचारिक चुनावों में तब्दील होते दिख रहे हैं. 2008 में माओवादी पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरे थे. शायद इसलिए कि लोग एक नई पार्टी को आजमाना चाह रहे थे और अन्य पार्टियां उस तरह मुखर होकर उनका भरोसा नहीं जीत पाई थीं. माओवादियों के सामने पहचान बनाने की चुनौती थी, जिसमें वे सफल भी रहे.
2013 आते-आते माओवादी दल अंतर्कलह का शिकार हो गए, जिसका लाभ नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल को मिला. आज वोटर तो अपने मुद्दे पहचानता है, लेकिन सारे दल मुद्दों से दूर होकर धन-बल का सहारा लेने को जूझते दिखाई दे रहे हैं. सच है कि नेपाल का पूरा सियासी परिदृश्य ही अजब संकट से जूझ रहा है. एक राजनेता की बात मानें, तो उन्हें जीतने के लिए कम से कम 5000 वोट की दरकार थी. सारे गुणा-गणित के बाद उनका निष्कर्ष था कि इतने वोट पक्के करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये तो खर्च करने ही होंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं पर अलग से दो करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा तमाम खर्च और.
आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें
डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप
- 24 प्रिंट मैगजीन
डिजिटल
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप