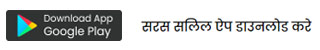Hindi Kahani: ‘टनटनटन...’ साइकिल की घंटी बजती तो दफ्तर के गार्ड विक्रम साहब की साइकिल को खड़ी करने के लिए दौड़ पड़ते. विक्रम साहब की साइकिल की इज्जत और रुतबा किसी मर्सडीज कार से कम न था. विक्रम साहब ठसके से साइकिल से उतरते. अपने पाजामे में फंसाए गए रबड़ बैंड को निकाल कर उसे दुरुस्त करते, साइकिल पर टंगा झोला कंधे पर टांगते और गार्डों को मुन्नाभाई की तरह जादू की झप्पी देते हुए अपनी सीट की तरफ चल पड़ते.
विक्रम साहब एक अजीब इनसान थे. साहबी ढांचे में तो वे किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठते थे या यों कहें कि अफसर लायक एक भी क्वालिटी नहीं थी उन में. न चाल में, न पहनावे में, न बातचीत में, न स्टेटस में. 90 हजार रुपए महीना की तनख्वाह उठाते थे विक्रम साहब, पर अपने ऊपर वे 2 हजार रुपए भी खर्च न करते थे. दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाने के अलावा उन्होंने दुनिया में कभी कुछ नहीं खाया था.
अपने मुंह से तो यह सब वे बताते ही थे, उन के डीलडौल को देख कर लगता भी यही था कि उन्होंने रूखी रोटी और सूखी सब्जी के अलावा कभी कुछ खाया भी नहीं होगा. काग जैसा रूप था उन का, पर अपनी बोली को उन्होंने कोयल जैसी मिठास से भर दिया था. औरतों के तो वे बहुत ही प्रिय थे. मर्द होते हुए भी औरतें उन से बेझिझक अपनी निजी बातें शेयर कर सकती थीं. उन्हें कभी नहीं लगता था कि वे अपने किसी मर्द साथी से बात कर रही हैं. लगता था जैसे अपनी किसी प्रिय सखी से बातें कर रही हैं. उन्हें विक्रम साहब के चेहरे पर कभी हवस नहीं दिखती थी.
आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें
डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप
- 24 प्रिंट मैगजीन
डिजिटल
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप