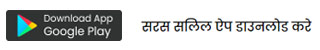मैं और मीना उस दुकान पर से उतर आए और जल्दी ही पूरा प्रसंग भूल भी गए. पता नहीं क्यों जब भी कहीं कुछ असंगत नजर आता है मैं स्वयं को रोक नहीं पाती और अकसर मेरे पति मेरी इस आदत पर नाराज हो जाते हैं.
‘‘तुम दादीअम्मां हो क्या सब की. जहां कुछ गलत नजर आता है समझाने लगती हो. सामने वाला चाहे बुरा ही मान जाए.’’
‘‘मान जाए बुरा, मेरा क्या जाता है. अगर समझदार होगा तो अपना भला ही करेगा और अगर नहीं तो उस का नुकसान वही भोगेगा. मैं तो आंखें रहते अंधी नहीं न बन सकती.’’
अकसर ऐसा होता है न कि हमारी नजर वह नहीं देख पाती जो सामने वाली आंख देख लेती है और कभीकभी हम वह भांप लेते हैं जिसे सामने वाला नहीं समझ पाता. क्या अपना अहं आहत होने से बचा लूं और सामने वाला मुसीबत में चला जाए? प्रकृति ने बुद्धि दी है तो उसे झूठे अहं की बलि चढ़ जाने दूं?
‘‘क्या प्रकृति ने सिर्फ तुम्हें ही बुद्धि दी है?’’
‘‘मैं आप से भी बहस नहीं करना चाहती. मैं किसी का नुकसान होता देख चुप नहीं रह सकती, बस. प्रकृति ने बुद्धि तो आप को भी दी है जिस से आप बहस करना तो पसंद करते हैं लेकिन मेरी बात समझना नहीं चाहते.’’
ये भी पढ़ें- मुखबिर
मैं अकसर खीज उठती हूं. कभीकभी लगने भी लगता है कि शायद मैं गलत हूं. कभी किसी को कुछ समझाऊंगी नहीं मगर जब समय आता है मैं खुद को रोक नहीं पाती हूं.
अभी उस दिन प्रेस वाली कपड़े लेने आई तो एक बड़ी सी गठरी सिर पर रखे थी. अपने कपड़ों की गठरी उसे थमाते हुए सहसा उस के पेट पर नजर पड़ी. लगा, कुछ है. खुद को रोक ही नहीं पाई मैं. बोली, ‘‘क्यों भई, कौन सा महीना चल रहा है?’’
‘‘नहीं तो, बीबीजी…’’
‘‘अरे, बीबीजी से क्यों छिपा रही है? पेट में बच्चा और शरीर पर इतना बोझ लिए घूम रही है. अपनी सुध ले, अपने आदमी से कहना, तुझ से इतना काम न कराए.’’
ये भी पढ़ें- Serial Story- कड़वी गोली
टुकुरटुकुर देखती रही वह मुझे. फिर फीकी सी हंसी हंस पड़ी.
‘‘पूरी कालोनी घूमती हूं, किसी ने इतना नहीं समझाया और न ही किसी को मेरा पेट नजर आया तो आप को कैसे नजर आ गया?’’
पता नहीं लोग देख कर भी क्यों अंधे बन जाते हैं या हमारी संवेदनाएं ही मर गई हैं कि हमें किसी की पीड़ा, किसी का दर्द दिखाई नहीं देता. ऐसी हालत में तो लोग गायभैंस पर भी तरस खा लेते हैं यह तो फिर भी जीतीजागती औरत है. कुछ दिन बाद ही पता चला, उस के घर बेटी ने जन्म लिया. धन्य हो देवी. 9 महीने का गर्भ कितनी सहजता से छिपा रही थी वह प्रेस वाली.
मैं ने हैरानी व्यक्त की तो पति हंसते हुए बोले, ‘‘अब क्या जच्चाबच्चा को देखने जाने का भी इरादा है?’’
‘‘वह तो है ही. सुना है पीछे किसी खाली पड़ी कोठी में रहती है. आज शाम जाऊंगी और कुछ गरम कपड़े पड़े हैं, उन्हें दे आऊंगी. सर्दी बढ़ रही है न, उस के काम आ जाएंगे.’’
‘‘नमस्कार हो देवी,’’ दोनों हाथ जोड़ मेरे पति ने अपने कार्यालय की राह पकड़ी.
मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहां गलत थी. मैं क्या करूं कि मेरे पति भी मुझे समझने का प्रयास करें.
कुछ दिन बाद एक और समस्या मेरे सामने चली आई. इन के एक सहयोगी हैं जो अकसर परिवार सहित हमारे घर आते हैं. 1-2 मुलाकातों में तो मुझे पता नहीं चला लेकिन अब पता चल रहा है कि जब भी वह हमारे घर आते हैं, 1 घंटे में लगभग 4-5 बार बाथरूम जाते हैं. बारबार चाय भी मांगते हैं.
बाथरूम जाना या चाय मांगना मेरी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उन के जाने के बाद हमारा बाथरूम चींटियों से भर जाता है. सफेद बरतन एकदम काला हो जाता है. हो न हो इन्हें शुगर हो. पति से अपने मन की बात बता कर पूछ लिया कि क्या उन से इस बारे में बात करूं?
‘‘खबरदार, हर बात की एक सीमा होती है. किसी के फटे में टांग मत डाला करो. मैं ने कह दिया न.’’
‘‘एक बार तो पूछ लो,’’ मन नहीं माना तो पति से जोर दे कर बोली, ‘‘शुगर के मरीज को अकसर पता नहीं चलता कि उसे शुगर है और बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाए तभी पेशाब में आती है. क्या पता उन्हें पता ही न हो कि उन्हें शुगर हो चुकी है.’’
‘‘कोई जरूरत नहीं है और तुम ज्यादा डाक्टरी मत झाड़ो. दुनिया में एक तुम ही समझदार नहीं हो.’’
ये भी पढ़ें- Short Story- एक कश्मीरी
‘‘उन्हें कुछ हो गया तो… देखो उन के छोटेछोटे बच्चे हैं और कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या उम्र भर हम खुद को क्षमा कर पाएंगे?’’
बेटे ने तो नजरें झुका लीं पर बाप बड़े गौर से मेरा चेहरा देखने लगा.
‘‘मेरे पिताजी भी इसी स्टूल पर पूरे 50 साल बैठे थे उन की पीठ तो नहीं दुखी थी.’’
‘‘उन की नहीं दुखी होगी क्योंकि वह समय और था, खानापीना शुद्ध हुआ करता था. आज हम हवा तक ताजा नहीं ले पाते. खाने की तो बात ही छोडि़ए. हमारे जीने का तरीका वह कहां है जो आप के पिताजी का था. मुझे डर है आप का बेटा ज्यादा दिन इस ऊंचे स्टूल पर बैठ कर काम नहीं कर पाएगा. इसलिए आप इस स्टूल की जगह पर कोई आरामदायक कुरसी रखिए.’’
अपने पति से जिद कर मैं एक दिन जबरदस्ती उन के घर चली गई. बातोंबातों में मैं ने उन के बाथरूम में जाने की इच्छा व्यक्त की.
‘‘क्या बताऊं, दीदी, हमारा बाथरूम साफ होता ही नहीं. इतनी चींटी हैं कि क्या कहूं इतना फिनाइल डालती हूं कि पूछो मत.’’
‘‘आप के घर में किसी को शुगर तो नहीं है न?’’
‘‘नहीं तो, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?’’
अवाक् रह गई थी वह. धीरे से अपनी बात कह दी मैं ने. रो पड़ी वह. मैं ने कहा तो मानो उसे भी लगने लगा कि शायद घर में किसी को शुगर है.