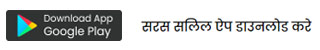देश में चुनावी शतरंज बिछ चुकी है। इस बार का लोकसभा चुनाव खुले तौर पर भाजपा और कांग्रेस के इर्द-गिर्द ही दिखायी दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के बीते पांच साल के कामकाज की धज्जियां उड़ाते हुए जगह-जगह जम कर बरस रहे हैं, वहीं नरेन्द्र मोदी प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में उतरने से बौखलाये हुए हैं। इसमें दोराय नहीं है कि प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतर पड़ने से इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोंकती नजर आ रही है। कांग्रेसियों का उत्साह आसमान पर है और यही वजह है कि कांग्रेस किसी गठबंधन में बंधे बिना अपने दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रही है। व्यंग्य बाण छोड़ने में माहिर नरेन्द्र मोदी ने हालांकि प्रियंका पर अभी तक सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, मगर कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप उन्होंने जरूर जड़ दिया है। वही पुराना घिसा-पिटा आरोप। कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। वंशवाद का आरोप कांग्रेस पर लम्बे समय से लगता आ रहा है मगर कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं होता। अब ये आलोचना की बात हो या प्रशंसा की, मगर सच्चाई यही है कि आज ‘कांग्रेस मतलब गांधी-परिवार’, बिल्कुल ‘ठंडा मतलब कोकाकोला’ की तर्ज पर। आज इस परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह परिवार कांग्रेस से जब-जब अलग हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई और कार्यकर्ताओं में बिखराव पैदा हुआ है। विपक्ष यह सोच कर वंशवाद का हो-हल्ला मचाता है कि शायद कुछ असर हो जाए और पुराने कांग्रेसी नेताओं के खून में उबाल आ जाये और गांधी परिवार के खिलाफ पार्टी के भीतर विरोध के अंकुर फूट जाएं, मगर विपक्ष का दांव हमेशा खाली ही जाता है क्योंकि कांग्रेस और गांधी एक सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं।
हालांकि एक वक्त था जब कांग्रेस और गांधी अलग-अलग थे। कांग्रेस और गांधी परिवार को एक करने का श्रेय जाता है इंदिरा गांधी को। वह वक्त था देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के बाद का। जब तक नेहरू जिन्दा थे, तब तक सरकार पर उनका एकछत्र राज था। उनके आगे कांग्रेस का वही हाल था, जो आज मोदी के आगे भाजपा का है। लेकिन नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को सक्रिय राजनीति से हमेशा दूर रखा था। यही कारण था कि उनकी मौत के बाद भारत की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया। तब शुरू हुई नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज। उस वक्त इंदिरा गांधी कहीं किसी गिनती में नहीं थीं। तब के. कामराज कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। वे तमिलनाडु से थे और दक्षिण भारत की निचली जाति के प्रभावशाली नेता माने जाते थे। मगर उनके दिमाग में भी इंदिरा का नाम दूर-दूर तक नहीं था। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद के जो दो मजबूत दावेदार थे वह थे – मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई को ज्यादातर कांग्रेसी पसन्द नहीं करते थे क्योंकि वे बड़े जिद्दी और अड़ियल किस्म के व्यक्ति थे, जबकि उनके विपरीत लाल बहादुर काफी शान्त और सौम्य थे। तब कांग्रेसी नेताओं ने एकमत से प्रधानमंत्री के रूप में लालबहादुर शास्त्री को चुना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चुना था। मगर शास्त्री जी मनमोहन सिंह नहीं बन पाये। यह कहानी कभी आगे, पहले इंदिरा की बात करें कि कैसे उनकी एंट्री कांग्रेस में हुई और कैसे आने वाले सालों में कांग्रेस और गांधी परिवार एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये।
दरअसल लालबहादुर शास्त्री ने ही पहली बार इंदिरा गांधी को अपने कैबिनेट में जगह दी थी। शास्त्रीजी इंदिरा की तेजी को समझते थे और जानते थे कि बाहर रह कर वह ज्यादा खतरनाक साबित होंगी, लिहाजा अपनी कैबिनेट में शामिल करके उन्होंने इंदिरा को कम महत्व वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री बना दिया। मगर इंदिरा को यह पद भाया नहीं। वे भीतर ही भीतर अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगी रहीं।
उसी दौरान शास्त्री जी चाहते थे कि वह तीन मूर्ति भवन स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हो जाएं, जहां जवाहरलाल नेहरू बतौर प्रधानमंत्री रहा करते थे, लेकिन इंदिरा ने इसमें अडंÞगा लगा दिया। वे चाहती थीं कि तीन मूर्ति भवन स्थायी तौर पर नेहरू के नाम का स्मारक घोषित हो जाए और आखिर में उन्हीं की जीत हुई। तीन मूर्ति भवन नेहरू और उनके वंशजों के नाम हो गया। उसके बाद इंदिरा की असल सियासत तीन मूर्ति से ही चलने लगी और ये परम्परा अब तक बरकरार है।
इंदिरा गांधी पार्टी के अन्दर अपनी ताकत बढ़ा रही थीं और लालबहादुर शास्त्री अकेले पड़ते जा रहे थे। तब शास्त्रीजी ने पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ खोला, जिसमें ईमानदार, विश्वासपात्र और काबिल अफसरों की टीम को देश चलाने के लिए रख लिया। पीएमओ का काम नाजुक और नीतिगत मसलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना था। शास्त्रीजी के इस पीएमओ वाले नये तजुर्बे ने इंदिरा के इशारे पर चल रहे कांग्रेसी नेताओं की चालें फेल कर दीं।
शास्त्रीजी की मौत के बाद कांग्रेस में फिर उत्तराधिकार की तलाश शुरू हुई। इस बार मोरारजी देसाई किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी काफी अनुभवी हो चुकी थीं। कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा का नाम आगे किया तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच चुनाव की नौबत आ गयी और अन्तत: कांग्रेस संसदीय दल के सांसदों ने इंदिरा को चुना और इंदिरा पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनीं। तब तक इंदिरा की उम्र 49 साल पार कर चुकी थी। अपनी मन्जिल तक पहुंचने में इंदिरा को लम्बा वक्त लग गया, मगर उनकी पोती प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजनीति की शुरुआत सत्ताइस साल की उम्र में कर दी थी, हालांकि यह राजनीति वे लगातार पर्दे के पीछे रह कर करती रहीं। सक्रिय राजनीति में वह अब उतरी हैं, 47 की उम्र में।
अगर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के लिए नेहरू-गांधी परिवार की समय सीमा निकालें तो आजादी के 70 साल में 53 साल तक इस परिवार का किसी न किसी पद पर या फिर दोनों पदों पर एक साथ कब्जा रहा है। वर्ष 1960 के दशक में नेहरू और इंदिरा (पिता-पुत्री), फिर 1970 के दशक में इंदिरा-संजय (मां-छोटे बेटे) और 1980 के दशक में इंदिरा-राजीव (मां-बड़े बेटे)। हालांकि बीच का कुछ वक्त था जब बाहरी व्यक्ति इन पदों पर सुशोभित हुए मगर उनसे पार्टी और कार्यकर्ताओं को उतनी मजबूती नहीं मिल पायी, जितनी गांधी परिवार के सदस्यों से मिलती है।
गांधी परिवार के बाहर से पहली बार किसी ने कांग्रेस को चलाया तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। राव ने 1996 तक कांग्रेस पार्टी और इसकी सरकार चलायी। 1996 से 1998 तक कांग्रेस के प्रमुख रहे गांधी परिवार के वफादार सीताराम केसरी पार्टी को साथ नहीं बांध सके थे और 1998 में कांग्रेस के विभाजन के बाद पार्टी की खस्ता हालत को देखते हुए सोनिया गांधी को न चाहते हुए भी कांग्रेस की मदद के लिए आगे आना पड़ा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान इसलिए संभाली क्योंकि उनके परिवार के बिना पार्टी डूब रही थी और पार्टी के बिना उनके परिवार की श्रेष्ठता और प्रासंगिकता खतरे में पड़ गयी थी। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना ही नहीं करते हैं। यही वजह है कि जब जब गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति ने पार्टी चलानी चाही, फेल हुआ। मनमोहन सिंह स्पष्ट तौर पर सोनिया की कठपुतली थी, इसलिए ही दस साल तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। मनमोहन सिंह की कलम से सोनिया के फैसले ही लिखे जाते रहे, इसमें कोई दोराय नहीं है, यदि वे ऐसा नहीं करते तो नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की भांति ही नकार दिये जाते। यह बात पार्टी के तमाम धुरंधर नेता भलीभांति समझते हैं कि पार्टी और कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ही एकजुट रख सकता है। यही वजह है कि शीर्ष पद के लिए कोई दावेदारी पार्टी नहीं उभरती। तो अगर पूरी पार्टी एक परिवार के नेतृत्व में एकजुटता के साथ रहे, इसमें बुराई क्या है?