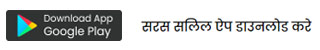9अप्रैल, 2023 की सुबह मैं अपने एक ठेकेदार दोस्त के साथ भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के चौराहे पर था. यह चौराहा मजदूरों के लिए मशहूर है. सुबह 7 बजे से मजदूर यहां जमा होने लगते हैं और 8-9 बजे तक पूरे इलाके में वही नजर आते हैं. कुछ झुंड बना कर खड़े रहते हैं, तो कुछ अकेले अलगथलग, जिस से आने वालों की नजर उन पर जल्दी पड़ सके.
ठेकेदार साहब मुझे समझाते रहे कि देखो, अभी ये लोग 500 रुपए मजदूरी दिनभर की मांगेंगे, लेकिन जैसे ही 10 बज जाएंगे, इन के भाव कम होते चले जाएंगे.
ठेकेदार को अपनी साइट पर काम करने के लिए 4-5 मजदूर चाहिए थे, लेकिन उन की निगाहें लगता था कि खास किस्म के मजदूरों को ढूंढ़ रही थीं. पूछने पर उन्होंने बताया कि वे आदिवासी मजदूरों को खोज रहे हैं, क्योंकि वे बहुत मजबूत, मेहनती और ईमानदार होते हैं. शहरी मजदूरों की तरह निकम्मे और चालाक नहीं होते, जिन्हें हर 2 घंटे बाद खानेपीने के लिए एक ब्रेक चाहिए. कभी उन्हें हाजत होने लगती है, तो कभी बीड़ीसिगरेट की तलब लग आती है. लंच भी वे लोग
2 घंटे तक करते रहते हैं. कुल जमा सार यह है कि शहरी मजदूरों से काम करा पाना आसान काम नहीं, क्योंकि वे कामचोर होते हैं.
फिर आदिवासी मजदूरों की खूबियां गिनाते हुए ठेकेदार बताने लगे कि वे कामचोरी नहीं करते और 200 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि शहरी मजदूर 400 रुपए से कम में हाथ भी नहीं रखने देते.
आदिवासी मजदूर को शाम को घर जाने के समय चायसमोसा खिला कर एक घंटे और काम कराया जा सकता है. और तो और लंच में उन्हें अचार और कटी प्याज के साथ सूखी रोटियां दे दो, तो वे एहसान मानते हुए मुफ्त में ऐक्स्ट्रा काम भी कर देते हैं.
इन ठेकेदार साहब की बातों और चौराहे का माहौल देख साफ हो गया कि आदिवासी वाकई में सीधे होते हैं और दुनियादारी से न के बराबर वाकिफ हैं. 400 रुपए का काम वे 200 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं, तो यह उन की मजबूरी भी है और जरूरत भी.
किराए की झुग्गी में रह रहे ऐसे ही एक गोंड आदिवासी परिवार से बात करने पर पता चला कि वे लोग बालाघाट से भोपाल काम की तलाश में आए थे और 6 महीने से बिल्डरों के यहां मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन नकद जमापूंजी के नाम पर कुल 800 रुपए हैं.
पूछने पर 35 साल के जनकलाल धुर्वे ने बताया, ‘‘हम पतिपत्नी और विधवा मां मजदूरी करते हैं. मुझे रोज 300 और उन दोनों को 200-200 रुपए मिलते हैं. इन पैसों से जैसेतैसे गुजर हो जाती है, लेकिन पैसे बचते नहीं हैं. मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते, क्योंकि यहां कोई दाखिला देने को तैयार नहीं है.
‘‘हर स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट और आधारकार्ड और पक्का पता वगैरह मांगा जाता है. आधारकार्ड तो हमारे पास है, लेकिन दूसरे जरूरी कागजात नहीं हैं, जिस के चलते सरकारी स्कूल वाले यह कहते हुए टरका देते हैं कि वहीं बालाघाट जा कर बच्चों का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दो.’’
लेकिन जनकलाल धुर्वे गांव वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां काम ही नहीं है. और जो है भी, वह तकरीबन बेगार वाला है. दिनभर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद मुश्किल से 100 रुपए मिलते हैं. कभीकभार सरकारी योजना के तहत मुफ्त राशन मिल जाता है, पर उस का कोई ठिकाना नहीं और उस से हफ्तेभर ही पेट भरा जा सकता है.
इसलिए गरीब हैं
आदिवासियों के पास पैसा क्यों नहीं है और वे गरीब क्यों हैं? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है, जिस का जवाब जनकलाल धुर्वे जैसे आदिवासियों की कहानी में मिलता है कि ये लोग पढ़ेलिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, जरूरत के मारे हैं. और भी कई वजहें हैं, जिन के चलते इस तबके की माली हालत आजादी के 75 साल बाद भी बद से बदतर हुई है.
भोपाल के एक आदिवासी होस्टल में रह कर बीकौम के पहले साल की पढ़ाई कर रहे बैतूल के प्रभात कुमरे की मानें, तो आदिवासी बहुल इलाकों में शोषण बहुत है, लेकिन उस से निबटना कैसे है, यह कोई नहीं बताता.
हम आदिवासियों को ले कर खूब हल्ला मचता है, करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, सरकार उन का खूब ढिंढोरा भी पीटती है, पर हकीकत में होताजाता कुछ नहीं है. आदिवासी तबका पहले से ज्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उस के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम हो रही है.
प्रभात कुमरे बहुत सी बातें बताते हुए आखिर में यही कहता है कि जो आदिवासी पढ़लिख कर सरकारी नौकरियों में लग गए हैं, वे ही चैन और सुकून से रह पा रहे हैं और उन्हीं के बच्चे अच्छा पढ़लिख पा रहे हैं. ऐसे लोग भी नौकरी मिलने के बाद अपने समाज की गरीबी दूर करने की कोई कोशिश या पहल नहीं करते हैं.
प्रभात कुमरे के मजदूर पिता जैसेतैसे उसे पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन के पास 2 एकड़ जमीन भी है. प्रभात कालेज पूरा करने के बाद किसी भी सरकारी महकमे में क्लर्क बन जाना चाहता है और यह आरक्षण के चलते उसे मुमकिन लगता है. इतने गरीब हैं
जनकलाल धुर्वे और प्रभात कुमरे की बातों से एक बात यह भी साफ हो जाती है कि पैसा गांवों में भी है और शहरों में भी है, लेकिन वह कम से
कम आदिवासियों के लिए तो बिलकुल नहीं है.
आदिवासियों के पास खेतीकिसानी की जमीन न के बराबर है और जो है, कागजों में वे उस के मालिक नहीं हैं. जिन जमीनों के पट्टे सरकारों ने आदिवासियों को दिए हैं, उन का रकबा इतना नहीं है कि वे आम किसानों की तरह उस से गुजर कर सकें.
मध्य प्रदेश में सब से ज्यादा कुल आबादी के 21 फीसदी आदिवासी हैं, जो तादाद में एक करोड़, 53 लाख के आसपास हैं. इस लिहाज से राज्य का हर 5वां आदमी आदिवासी है.
इन में से 85 फीसदी के आसपास खेतिहर मजदूर हैं, जो जंगलों में रह कर रोज कुआं खोद कर पानी पीने को मजबूर हैं. इन की आमदनी जान कर हैरत होती है कि इतने कम पैसों में ये गुजर कैसे कर लेते हैं.
कोई अगर यह सोचे कि भला धर्म, जाति और लिंग का आमदनी से क्या ताल्लुक, तो उसे एक रिपोर्ट पढ़ कर अपनी यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए.
दुनियाभर से भेदभाव दूर करने का बीड़ा उठाने वाली संस्था ‘औक्सफेम इंडिया’ की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सवर्णों की मासिक आमदनी एससी यानी दलित और एसटी यानी आदिवासियों से औसतन 5,000 रुपए ज्यादा है.
इस रिपोर्ट के मुताबिक, शहरों में एससी और एसटी तबकों की नियमित कर्मचारियों की औसत कमाई 15,312 रुपए है, जबकि सामान्य तबके के लोगों की कमाई 20,346 रुपए है. यह फर्क तकरीबन 33 फीसदी है.
अगर दलित और आदिवासी अपना खुद का काम करते हैं, तो उन की औसत कमाई 10,533 रुपए रह जाती है, जबकि खुद का काम करने वाले सामान्य तबके के लोगों की कमाई उन से एकतिहाई ज्यादा यानी 15,878 रुपए महीना होती है.
यह रिपोर्ट उन दावों की कलई भी खोलती है, जिन के हल्ले के तहत यह माना जाता है कि आदिवासियों को तो सरकार मुफ्त के ब्याज पर खूब कर्ज देती है, जबकि रिपोर्ट खुलासा करती है कि खेतिहर मजदूर होने के बाद भी आदिवासियों को खेतीकिसानी का लोन आसानी से नहीं मिलता और जिन्हें जैसेतैसे मिल भी जाता है, तो वह सामान्य तबके के लोगों के मुकाबले एकचौथाई होता है.
ज्यादातर आदिवासियों के पास चूंकि जमीन के पक्के और पुख्ता कागज नहीं होते, इसलिए उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिल पाता. ‘कर्जमाफी’ या ‘किसान सम्मान निधि’ के हकदार ये लोग नहीं हो पाते.
पीढि़यों से वनोपज बीनबीन कर बेचने वाले आदिवासी अपनी मेहनत के वाजिब दाम कभी नहीं ले पाए. जो महुआ, चिरौंजी और तेंदूपत्ता ये लोग बीनते हैं, उस की बाजार में कीमत अगर एक रुपया होती है, तो इन्हें 15 पैसे ही मिलते हैं यानी दलाली सरकारी ही नहीं, बल्कि गैरसरकारी तौर पर भी इन की कंगाली की बड़ी वजह है. दूसरे, शराब की लत की भी कीमत आदिवासी चुका रहे हैं, जो इन से छूटती नहीं.
ऊपर बैठे हैं ऊंची जाति वाले
हकदार तो बहुत सी योजनाओं के लिए आदिवासी इसलिए भी नहीं हो पाते, क्योंकि नीचे से ले कर ऊपर तक इन से ताल्लुक रखते महकमों में वे ऊंची जाति वाले हिंदू विराजमान हैं, जो हमेशा से इन्हें हिकारत और नफरत से देखते आए हैं.
धर्म और समाज दोनों आदिवासियों को जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते. इन की बदहाली की वजह पिछले जन्म के कर्म माने जाते हैं, इसलिए ये ऊपर वाले और ऊपर वालों की ज्यादती के शिकार हमेशा से ही रहे हैं.
पटवारी से कलक्टर और उस से भी ऊपर के ओहदों पर सवर्ण अफसरों का दबदबा है. मिसाल मध्य प्रदेश की लें,
तो आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में प्रबंध संचालक जैसे अहम पद पर 25 सालों से ज्यादातर सवर्ण और उन में भी ब्राह्मण अफसर काबिज हैं, जिन की दिलचस्पी आदिवासियों के न तो वित्त में है और न ही हित में है.
इन अफसरों को न तो जनकलाल धुर्वे जैसों को कम मिल रही मजदूरी से मतलब है और न ही ये प्रभात जैसे नौजवानों से कोई सरोकार रखते हैं, जिन्हें कभीकभी फीस भरने और खानेपीने तक के लाले पड़ जाते हैं.
इन अफसरों ने आदिवासियों की जिंदगी भी नजदीक से नहीं देखी होगी कि वे एकएक कागज के लिए दरदर सालोंसाल भटकते रहते हैं, लेकिन उन की कहीं भी सुनवाई नहीं होती.
रही बात आदिवासियों से ताल्लुक रखते महकमों की, तो हाल यह है कि घूसखोर मुलाजिम इन गरीबों का खून चूसने में खटमलों की तरह चूकते नहीं.
11 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के ही रतलाम जिले के गांव भूतपाड़ा में एक पटवारी सोनिया चौहान ने रमेश नाम के एक आदिवासी को फर्जी पावती टिका दी और हैरत की बात यह कि उस के भी बतौर घूस एक लाख, 90 हजार रुपए झटक लिए.
कैसे सीधेसादे आदिवासी सरकारी सिस्टम, जिस पर सवर्णों का कब्जा है, की मार झेल रहे हैं और कैसे देशभर में सरकारी जमीनों को प्राइवेट करने का फर्जीवाड़ा फलफूल रहा है, यह इस मामले से भी उजागर होता है.
रमेश जब जमीन के खाते और खसरे की नकल लेने तहसील पहुंचा तो पता चला कि जो जमीन उस के नाम दर्ज की गई है, वह तो सरकारी निकल रही है. उस की शिकायत पर पटवारी साहिबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जिस ने किस्तों में घूस लेने के अलावा रमेश से अपने घर मेहनतमजदूरी भी कराई थी.
प्रभात कुमरे की कही बात मानें, तो आदिवासियों के ज्यादातर काम सरकारी महकमों से ही होते हैं. लेकिन मजाल है कि ये बाबू और साहब लोग बिना रिश्वत लिए कोई काम कर दें. जाति प्रमाणपत्र बनवाने से ले कर किसी भी सरकारी योजना का फायदा बिना दक्षिणा चढ़ाए नहीं मिलता.
अशिक्षा है वजह
आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के ही एक ऊंची जाति वाले क्लर्क की मानें, तो आदिवासी जब तक अशिक्षित रहेंगे, तब तक गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे अपने हक ही नहीं जानते, इसलिए कहीं भी ज्यादती का विरोध नहीं कर पाते. सरकार इन के भले की योजनाओं पर जो अरबों रुपए खर्च कर रही है, उस का
90 फीसदी तो घोटालों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है. यहां यानी भोपाल से सरकार अगर पोल्ट्री फार्म उन्हें भेजती है, तो उन तक एक अंडा ही पहुंचता है और यह हकीकत नीचे से ऊपर तक सभी जानते हैं. मतलब, योजनाएं आदिवासियों के भले के लिए नहीं, बल्कि नेताओं, अफसरों और मुलाजिमों के कल्याण के लिए बनती हैं. अनपढ़ और अशिक्षित रहने से नुकसान क्या होते हैं, यह आदिवासियों को समझाने वाला कोई नहीं है, जिन के 99 फीसदी से भी ज्यादा नौजवान कालेज का मुंह नहीं देख पाते.
प्राइमरी स्कूलों में टीचरों का न जाना अब मीडिया के लिए भी हल्ला मचाने की बात नहीं रही, क्योंकि उन्होंने भी धर्म के शातिर ठेकेदारों की तरह मान लिया है कि आदिवासी ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे, इन के लिए आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं.