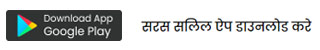कठुआ बलात्कार कांड के बाद लोगों का ध्यान कश्मीर की घुमंतु जनजाति बकरवाल की तरफ गया. मगर इस जनजाति पर फिल्मकार पवन कुमार शर्मा ने एक फिल्म ‘ ‘करीम मोहम्मद’’ का निर्माण किया है, जो कि कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद 24 अगस्त को सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है. पवन कुमार शर्मा की फिल्म ‘‘करीम मोहम्मद’’ का कठुआ कांड से कोई संबंध नही है, मगर उनकी फिल्म बकरवाल जनजाति के लोगों के जीवन पर रोशनी डालने के साथ ही इस बात को चित्रित करती है कि किस तरह इस समुदाय के लोग उंची पहाड़ियों पर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखते हुए भारतीय फौज की मदद करता है. यानी कि बकरवाल एक देशभक्त जनजाति है.

प्रस्तुत है पवन कुमार शर्मा से हुई लंबी बातचीत के अंश…
आपकी पृष्ठभूमि क्या है?
मैं हिमाचल में मंडी से हूं. पहाड़ों पर ही पला बढ़ा हूं. 20-22 साल तक वहां के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी. पर वहां थिएटर हैं. थिएटर ही हमें यहां तक लेकर आया. 1985 में एनएसडी की तरफ से मंडी में एक एक्टिंग वर्कशाप आयोजित हुआ था, जिसमें मैं व रोहिताश्व गौड़ सहित कई लोग जुड़े थे. वहीं से हम सभी ने अपने अपने रास्ते चुने. जब मैंने वहां से दिल्ली आने का निर्णय लिया, तो मेरी मां ने बहुत रोना धोना मचाया. हमें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली है. हमारे अंदर काफी जुझारू पन है. हमने काफी लड़ाई लड़ी. लड़ते लड़ते या यूं कहे कि संघर्ष करते करते यहां तक पहुंचे हैं. अभी भी हम समझौता वादी काम नहीं कर रहे हैं. लड़ाई जारी है. मेरे लिए फिल्म निर्माण पूजा है. मेरी नयी फिल्म ‘करीम मोहम्मद’ एक हवन है, जिसमें सभी कलाकारों व तकनीशियनों ने अपनी अपनी आहुती दी है.
काफी लंबे समय के बाद आपने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा. इसकी कोई खास वजह?
देखिए, मुंबई नगरी में हर कोई फिल्म अभिनेता बनने के लिए आता है. मैंने भी 1986 से 1989 तक एनएसडी से अभिनय की ट्रेनिंग ली थी. मेरे साथ संजय मिश्रा भी थे. मैंने अभिनय में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है. कुछ अवार्ड भी मिले थे. हम तो सोच रहे थे कि हमें अभिनेता बनना है, पर नियति और फिल्म इंडस्ट्री क्या चाहती है, हमें पता नहीं होता है. यह इंडस्ट्री आपको मेकअपमैन या स्पाट ब्वाय या प्रोडक्शन वाला या अभिनेता या निर्देशक बनाती है. फिल्म इंडस्ट्री में आपकी इच्छाएं नहीं चलती. इच्छाएं उन्ही की चलती हैं, जिन्हें संघर्ष करने के लिए बीस वर्षो तक घर से पैसा आ रहा हो. हां! कभी किसी का तुक्का भी लग जाता है. अन्यथा बौलीवुड में अभिनेता बनना आसान नही है. यहां लोग अभिनेता बनने आते हैं और बन कुछ और जाते हैं. ऐसा ही मेरा भी मसला है. मैं भी यहां अभिनेता बनने ही आया था. इसके अलावा आपकी अपनी शिक्षा पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह के जानर में आपको काम करने की इजाजत देती है, वह भी मायने रखता है. हर इंसान हर काम नही कर सकता. जैसा कि मैं प्राईवेट चैनल के लिए सास बहू जैसा सीरियल नहीं बना पाया. इसलिए मैंने अपने मनपसंद का काम करने का एक रास्ता खोजा. मैंने पंकज कपूर के साथ बतौर सहायक निर्देशक काम किया. इसके अलावा मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं जो भी काम करूं, वह बक्से में बंद ना रहे. लोगों के सामने आए.
यानी कि आपने स्वतंत्र रूप से निर्माण व निर्देशन किया है?
जी हां! बतौर निर्माता निर्देशक दूरदर्शन के लिए 30 से 40 सीरियल बनाए. जिसमें मेरा सबसे ज्यादा चर्चित सीरियल रहा मुल्कराज आनंद की कहानी पर बना ‘एक सूरमा की मौत’. इसके अलावा ‘विलेजेस हियर एंड देयर’ की. जिसमें मैंने दिखाया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गांवों में हालात कैसे हैं और पाक सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र के गांवों की हालत कैसी है. पाकिस्तानी लगातार कश्मीर का राग अलापता है, पर वह हमें बताए कि आजादी के इतने साल बाद वह पाक आधिकृत कश्मीर के गांव के लिए क्या कर पाए? हमारे यहां अकनूर हो या कोई दूसरा गांव, वहां पर सड़के बनी हैं. सारी सुविधाए हैं. पर उधर झांक कर देखो बहुत बुरी हालत है. जब आप उसे नही संभाल पा रहें हैं, तो कश्मीर को क्या संभालेंगे. कश्मीर की एक बहुत बड़ी संत रही हैं लाल डेद. जिस तरह से कबीर ने दोहे लिखे हैं, उसी तरह से वह भी लिखा करती थीं. उन पर मैंने सीरीज बनायी. ‘अफगान रूल इन कश्मीर’ पर एक सीरीज बनायी. किसी को यह बात पता नही है कि कश्मीर पर कभी अफगान ने शासन किया था. ‘मुगल रूल इन कश्मीर’ पर भी एक सीरीज की थी. जब डिजीटल आया, तो मैंने सोचा कि डिजीटल में ऐसे काम करना ठीक नही होगा. इसलिए मैंने सबसे पहले पोस्ट प्रोडक्शन का सेटअप बनाते हुए संकलन स्टूडियो शुरू किया. डिजीटल विद्या को सीखा. समझ में आया कि कैसे हम कम पैसे और कम साधन के साथ एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं. मैं जोड़तोड़ वाली फिल्म बनाने में यकीन भी नहीं करता. मेरा मानना है कि अभिनेता व निर्देशक जितनी साधना करता है, उसका काम उतना ही निखर कर आता है. एक फिल्म तो एक माह में बन जाती है, पर उसमें चालीस साल की साधना भी होती है. हम यह भूल जाते हैं. हर निर्देशक अपनी पहली फिल्म में अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ डाल देता है. उसके बाद की फिल्मों में फिर से बहक जाता है. मैंने अनुभव से सीखा है कि अभाव में जो काम बेहतर हो सकता है, वह सुविधाएं आने के बाद नहीं हो सकता. क्योंकि अभाव के बीच सपनों को पूरा करने का इंसान का जो जुनून होता है, वह कमाल का होता है.
आप भी एनएसडी से हैं. लेकिन पहले देखा गया था कि एनएसडी से आने वाले कलाकार मैथड एक्टिंग सीख कर आ रहे थे और फिल्मों में असफल हो रहे थे?
हर कलाकार को समझना होगा कि फिल्म और थिएटर मिले हुए भी हैं, तो वहीं दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं. दिमागी सोच व प्रशिक्षण के स्तर पर दोनों एक हैं, पर दोनों का ग्रामर अलग है. जैसे कि हिंदी में भी कई तरह की बोलियां हैं. इसी तरह से थिएटर व फिल्म दोनों की भाषाएं अलग हैं. इस बात को हर कलाकार को समझना पड़ेगा. थिएटर में जब आप संवाद अदायगी करते हैं, तब सामने बैठे अंतिम इंसान तक आपकी आवाज जानी चाहिए. पर सिनेमा में यही लाउड एक्टिंग हो जाती है. एनएसडी की ट्रेनिंग आपको एक अभिनेता के तौर पर तैयार करती है. पर फिल्मों से जुड़ने के लिए आपको फिल्म विधा को भी समझना पड़ेगा. फिल्म निर्माण की अपनी अलग कार्यशैली है. फिल्म के ग्रामर को समझने के लिए आपको कैमरे के लेंस, कैमरा एंगल, राइट लेफ्ट वगैरह सब कुछ समझना पड़ेगा. एनएसडी से आने वाले जिन कलाकारों ने फिल्म के ग्रामर को सीखा, वह सफल हो गए. कलाकार हो या निर्देशक दोनों के लिए फिल्म हो या थिएटर दोनों के अंतर को समझना जरूरी है.

आपने अब तक जो काम किया है, वह ज्यादातर कश्मीर केंद्रित रहा है. इसकी कोई खास वजह?
इसकी वजह है पहाड़. हिमाचल और कश्मीर में लोकेशन को देखते हुए कोई फर्क नही है. हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी हिस्से में जाएं, तो वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है. हम जहां पले बढ़े होते हैं, वह कहीं न कहीं हमारे दिलों दिमाग में छाया रहता है. मेरा पहाड़ीपन का अपना एक जानर है. इसके अलावा हमारी फिल्मों में बजट ज्यादा नहीं होता. यदि हम मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग करते हैं, तो हमें लोकेशन के किराए के रूप मे लंबी रकम देनी पड़ती है. पर हिमाचल प्रदेश में हमें वही लोकेशन मुफ्त में मिल जाता है. जबकि हिमाचल प्रदेश में ‘यशराज फिल्मस’ वालों को लोकेशन के पैसे देने पड़ेंगे. तो लोकेशन की कीमत कम हो जाने के कारण हमारे लिए हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में जाकर काम करना आसान हो जाता है. वहां अपने लोग हैं. तो वह हमें मदद करते हैं. इसके अलावा हम जहां से आए हैं, वहां के लिए कुछ करने का हमारा एक कर्ज होता है, जिसे हम चुकाते हैं. हम अपनी फिल्मों में वहां की लोकेशन ही नहीं, वहां के पेड़, पौधे, ट्रैक्टर व कलाकारों को भी हिस्सा बनाते हैं. इसके साथ ही हम हिमाचल व कश्मीर की नई पीढ़ी के लिए राह भी दिखाना चाहते हैं कि वह वहां रहकर भी काम कर सकते हैं. इसलिए मेरी फिल्म व टीवी सीरीज में पहाड़ मुख्य मुद्दा होता है.
फिल्म ‘‘करीम मोहम्मद’’ क्या है?
यह कश्मीर में बकरवाल जाति की रोड ट्रिप वाली फिल्म है. जिसमें एक बच्चे के नजरिए से आतंकवाद, जिंदगी, शिक्षा, जमीर सहित कई सवालो के जवाब तलाशने की कोशिश की गयी है. हमारी फिल्म बताती है कि किस तरह कुछ लोग चुनौती लेकर जिंदगी को छोड़कर जमीर की सुनते हैं. लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर के लोग अपने जमीर के लिए क्या क्या करते है. किस तरह का त्याग करते हैं. फिल्म ‘करीम मोहम्मद’ कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है.
आपने अपनी फिल्म की कहानी के लिए बकरवाल जनजाति को ही क्यों चुना?
अब जब आसीफा कांड आया, तो बकरवाल जाति का जिक्र आया. जबकि मैं राजस्थान के गुर्जरों पर डाक्यूमेंटरी बनाते समय इन बकरवाल जाति के संपर्क में आया था. यह राजस्थान के गुर्जर ही हैं जो कि कश्मीर में जाकर बसे हैं. गुर्जरों को सब जानते हैं, पर बकरवाल को कोई नहीं जानता. जबकि बकर वालों की जिंदगी बहुत कठिन है. इनकी सारी शिक्षा यात्रा करते हुए ही होती है. करीम का पिता पढ़ा नहीं है, मगर उसके पास हर सवाल का जवाब है. न्यूटन का सिद्धांत प्रकृति से आ सकता है, तो पिता के पास सवाल के जवाब क्यों नही हो सकते?
हमारी फिल्म में जब बेटा अपने पिता से पूछता है कि बापू आप तो मदरसे गए नहीं, तो आपको यह ज्ञान कहां से आया? तो पिता कहता है कि कायनात /प्रकृति ही सिखाती है. प्रकृति की शिक्षा सशक्त होती है. जब भेड़ की टांग टूट जाती है, तो पिता को पता है कि उसका इलाज कैसे करना है.

आपकी फिल्म ‘करीम मोहम्मद’ में कश्मीर की समस्या है.आपने कैसे कश्मीर को नजदीक से समझा?
देखिए, कश्मीर का जो मूल मुददा है, उसे हम जरूरत से ज्यादा जटिल बनाते जा रहे हैं. हम लोग एक तबके को बहुत अलग नजरिए से देखने लगे हैं. मैं खुद कश्मीर में काफी समय रहा हूं. मैंने पाया कि पूरा कश्मीर ऐसा नहीं है. कश्मीर का एक छोटा सा इलाका दहशतगर्दों व पत्थरबाजों से जुड़ा हुआ है. पर इसके लिए हमने पूरे कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना दिया, यह गलत है. हम पूरे मुस्लिम तबके को दोषी ठहराएं, यह भी गलत है. मेरी राय में आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता. इसलिए आतंकवाद के नाम पर किसी समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए. आतंकवाद का ना तो धर्म होता है, ना चेहरा और न जगह होती है. समस्या आसाम में भी है. सीरिया में भी है. लंदन, चीन, अमरीका सहित हर जगह समस्याएं हैं. तो हम सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का राग अलापते रहेंगे, तो हम कश्मीर के जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, उनकी भी हम तौहीन कर रहे हैं. ऐसी ही एक कम्यूनिटी बकरवाल है, जिसका दर्द हमने नहीं देखा, जो कि हिंदुस्तान के अंदर सेना की मदद करते रहते हैं. वह ऐसी उंचाई पर जाते हैं, जहां हमारे देश के सैनिक भी नहीं जाते हैं. बकरवाल जाति के यह लोग बाकायदा देश के सैनिकों को जानकारी देकर मदद करते रहते हैं. यह सरहद पर जवान की तरह खड़े रहते हैं, जबकि इनकी भेड़ बकरी व खाना छीन लिया जाता है. इनकी बहू बेटियों का अपमान किया जाता है. इस समुदाय को आगे लाना भी हमारा फर्ज व मकसद बनता है. हम चाहते हैं कि कश्मीर समस्या को लेकर एक सार्थक बहस शुरू हो. इससे पहले भी मैने कश्मीर को लेकर जो काम किया, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है.वहां की संत लाल डेद को लोग जानते ही नहीं हैं. वहां के ज्यादातर जहीन लोगों की अच्छाई को सामने लाना जरुरी है. वह हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है.
मेरी फिल्म ‘‘करीम मोहम्मद’’ में कहीं कोई गोली बारूद नहीं है. पूरी फिल्म बच्चे के नजरिए से आगे बढ़ती है और कश्मीर का जो दूसरा पहलू है, उसे पूरा विश्व देख सकेगा. हम कश्मीर का राग अलापते हुए सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं. जबकि वहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है. वहां थिएटर हो रहा है, फिल्में बन रही है. कई अच्छे नाटक हो रहे हैं. थिएटर जगत में भवन बशीर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम उनके बारे में बात क्यों नही करते. उन्हें भी आतंकवाद का सामना करना पड़ा. मेरा मकसद कश्मीर के सकारात्मक पक्ष के बारे में बात करना है.
छोटी फिल्मों को थिएटर नही मिल पाते हैं. इसका तोड़ क्या हो सकता है?
वर्तमान समय की यह सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसे हम सभी फिल्मकार व हमारी एसोसिएशन लड़ रही हैं. मैं एक फिल्म फेस्टिवल में गया था, वहां मुझे एक 72 साल का विदेशी पत्रकार एलेक्स मिली, तो उसने कहा भारतीय सिनेमा में नक्ली काम ही नजर आता है. उसने कहा भारतीय सिनेमा में भारत तो कहीं नजर ही नहीं आता. तो जब हमें अपने ही सिनेमा में अपने ही देश को दिखाने में समय लग रहा है, तो क्या होगा? जब सत्यजीत रे ने अपनी फिल्मों में भारत को दिखाया, तो उनकी फिल्में आस्कर अवार्ड तक पहुंची. पूरे विश्व में लोग सत्यजीत रे को जानते हैं. पर हम सभी तो हालीवुड की नकल करने में लगे हुए हैं.जिस दिन हम भारतीय सिनेमा में भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ भारतीय कहानियों को दिखाएंगें,फिल्मों में भारतीय समस्या को लेकर चलेंगें, हमारा सिनेमा उपर जाएगा. मैं तो इसी तरह के सिनेमा में विश्वास करता हूं. मेरी फिल्म ‘करीम मोहम्मद’ भी उसी तरह की है. इसके लिए जरूरी है कि देश में अच्छे अच्छे फिल्म फेस्टिवल हों. हमारे यहां नकली फिल्म फेस्टिवल बहुत चल रहे हैं. सरकार को चाहिए कि ऐसे फिल्म फेस्टिवलों पर रोक लगाए. ऐसे फिल्म फेस्टिवलों पर रोक लगनी चाहिए, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए चल रहे हैं. जब अच्छे फिल्म फेस्टिवल होंगे, तो सिनेमा अच्छा बनेगा.पर सिनेमा बनना रूकना नही चाहिए. यदि 100 घटिया फिल्में बन रही हैं, तो 10 अच्छी फिल्में भी बननी चाहिए. यदि इसी तरह से ‘आखों देखी’, ‘मुक्तिभवन’, ‘कड़वी हवा’, ‘करीम मोहम्मद’ जैसी फिल्में बनती रहीं, तो वह दिन दूर नही, जब यही मेन सिनेमा होगा. हमारा नाच गाना वाला फूहड़ सिनेमा पैरलल सिनेमा बनकर रह जाएगा. सिनेमा एक ऐसा प्रोफेशन है, जहां सिर्फ पैसे के लिए काम नही किया जाता. फिल्मकार की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, उसे भी उसे निभाना चाहिए. एक दिन वह आएगा, जब सिनेमाघर वाले छोटी छोटी फिल्मों को बुलाकर लोगों को दिखाएंगे. हमारी फिल्म को थिएटर मिल रहे हैं. देखना यह है कि दर्शक कितने पहुंचते हैं. जरुरत है कि दर्शक भी 100 या 200 रूपयों की आहुति नेक काम में डाले. दर्शक ही सिनेमा घर के मालिकों को अच्छी फिल्म दिखाने के लिए दबाव डाल सकते हैं.