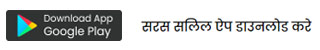आजाद भारत केवल वह सपना नहीं था, जिस में देश को अंगरेजों की गुलामी से आजाद कराने का रास्ता तय करना था, बल्कि यह सपना उस आजादी का भी था, जिस में देश के हर नागरिक को इज्जत से जीने का हक हासिल हो सके.
आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी इस बात को आज कोई भी दावे से नहीं कह सकता है कि देश के हर नागरिक को इज्जत की जिंदगी जीने का हक हासिल है.
इस देश में आज भी गरीब आदिवासी और पिछड़ेदलित अपनी इज्जत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. आदिवासियों को आज भी यह भरोसा नहीं है कि उन के जल, जंगल और जमीन में वे रह सकेंगे.
जिस तरह आजादी के बाद की सरकारों ने तरक्की के नाम पर खेती की जमीनों के कब्जे को बढ़ावा दिया है और आदिवासियों को उन की जगह से जबरन हटाया है, उस से उन कीदहशत सामने आई है.
यह कैसा आजाद देश है, जहां की दोतिहाई से ज्यादा आबादी एक दिन में 50 रुपए भी नहीं कमा पाती है? आजादी के इतने साल बाद भी गरीबी, बेरोजगारी, पढ़ाईलिखाई, इंसाफ देश के सामने बड़े सवाल बन कर खड़े हैं. जिन क्षेत्रों में तरक्की हुई दिखाई पड़ती है, वहां पर भी भ्रष्टाचार और भाईभतीजावाद ने आम लोगों की राह रोक रखी है.
आखिर इस देश में एक रिकशे वाले, एक मजदूर, एक गरीब या खेती करने वाले के बच्चों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुना जाना या खेल में इंटरनैशनल लैवल पर मैडल लाना महिमामंडन वाली खबरें क्यों हैं? वजह, हम ने देश में उस ढांचे का विकास ही नहीं किया है, जिस में देश के अमीर और गरीब दोनों के बच्चों के लिए बराबरी के मौके और सुविधाएं मुहैया हों.
देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का बचपन ही भेदभाव से रूबरू करा देता है. एक तरफ सारी सुविधाओं से लैस अंगरेजी भाषा वाला बचपन होता है, जिस की पढ़ाईलिखाई सत्ता की भाषा में होती है. वहीं दूसरी तरफ नंगे पैर वाला टाटपट्टी पर इलाकाई भाषा में पढ़ने वाला बचपन, जो प्रतियोगी माहौल में पहुंचने पर पाता है कि उस ने जिस भाषा में लिखापढ़ा है, वह भाषा न तो बड़ीबड़ी कंपनियों में चलती है और न ही सार्वजनिक उपक्रमों में.
यहां तक कि उस भाषा में बड़ी अदालतों में भी न तो याचिका दाखिल की जा सकती है और न ही बहस की जा सकती है. इस का मतलब तो यही है कि इंसाफ पाने के अधिकार से ले कर आजीविका तक के अधिकार से देश की एक बड़ी आबादी दूर है.
एक गरीब के लिए इंसाफ की पहली लड़ाई न्यायपालिका के रूढि़वादी कानूनी तरीकों और जजों से निबटने से ही शुरू हो जाती है. जनता और न्यायपालिका के बीच बहुत दूरी है. इस देश में अभी भी उन्हीं कानूनों से जनता को हांका जा रहा है, जिसे अंगरेजों ने 19वीं सदी में बनाया और लागू किया था.
हमारे देश की पुलिस और न्यायपालिका कानून व्यवस्था की अंगरेजी प्रणाली और सोच से आज भी नहीं उबर सकी हैं. गुनाह और सजा से रिश्ता सिर्फ ऐसे लोगों का है, जिन के पास पैसा नहीं है, जिन का कोई रसूख नहीं है और जो काफी मेहनत कर के भी जिंदगीभर गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं.
सवाल उठता है कि अगर महज 8 से 10 साल के भीतर गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइटें देश की हर भाषा में बात करने की भाषाई क्रांति ला सकती हैं, तो आधुनिकतम संसाधनों, तकनीकों और सुविधाओं से लैस हमारी संसद क्यों नहीं?
सोशल साइटों की भाषाई क्रांति ने साबित कर दिया है कि भाषा के मामले में हम ने अंगरेजी के दबदबे को कायम रखने के लिए देश की जनता के साथ तकरीबन 70 साल से धोखा किया है.
आज आम परिवार के बच्चों का राजनीति में आना मुश्किल हो गया है. परिवारवाद की राजनीति का कोढ़ देश की हर पार्टी में फैल चुका है और आलम यह?है कि देश की जनता को आज गुमराह किया जा रहा है कि देश में युवा नेतृत्व आ रहा है. किसे नहीं पता कि
यह युवा नेतृत्व नहीं, बल्कि परिवार नेतृत्व है. देश की सारी समस्याएं और मुद्दे छोड़ कर राजनीतिक दल धर्म और क्षेत्र की राजनीति करने में लगे हैं. आज किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि, सांसद या विधायक की अपनी आवाज का कोई वजूद नहीं है. अगर पार्टी नहीं चाहती?है, तो वह सदन में किसी विधेयक पर अपनी निजी राय भी नहीं रख सकता है.
वैसे, इस की शुरुआत तो टिकट के बंटवारे के साथ ही हो जाती?है. इस से बड़ी खतरनाक बात क्या होगी कि जो लोग जनता की नुमाइंदगी नहीं हासिल कर पाते हैं, उन्हें भी सरकार में शामिल कर लिया जाता है.
देश आजाद हो गया है, लेकिन उस के साथ आजाद हुए केवल अमीर और रईस लोग. किस सरकार में दम है कि इन के हितों के खिलाफ जा कर भूमि सुधार लागू कर सके? नक्सलवाद के खिलाफ गोली उगलने वाली सरकार बता सकती है कि क्यों उस के अपने ही देश के नागरिक देश के भीतर अपनी अलग व्यवस्था बना कर रखे हुए हैं?
आखिर अमीरों के पैर दबादबा कर गरीबों के इस जख्म को नासूर किस ने बनने दिया? जो सरकार हकों का बंटवारा करने के नाम पर गरीबों का हक छीन कर अमीरों में बांटती हो, उस की खिलाफत किस बिना पर गलत कही जा सकती है?
आज भी जिस तरह से दलितों पर जोरजुल्म की खबरें देखनेसुनने को मिल रही हैं, उसे राजनीतिक मुद्दा कह कर खारिज नहीं किया जा सकता है.
ऊंचेतबके का एक बड़ा हिस्सा दलितों और आदिवासियों को आजादी के इतने साल बाद भी हिकारत की नजर से देखता है, उस के मुख्यधारा में आने की कोशिशों को नाकाम करने में लगा हुआ है. ऐसा समाज चाहता है कि दलित और आदिवासी समझे जाने वाले लोग ही काम करते रहें और उन का पहले की तरह शोषण किया जाता रहे.
शायद लोग भूल चुके हैं कि देर से ही सही, पर वाकई संचार क्रांति ने सामाजिक उथलपुथल की एक नई संस्कृति लिखी है, जिस को सैंसर करना अब किसी भी सरकार के बस के बाहर की बात है.
यह सोशल मीडिया का दबाव ही है कि देश के प्रधानमंत्री को दलित उत्पीड़न मामलों पर सामने आ कर सरकार का पक्ष रखने को मजबूर होना पड़ा है, इसलिए जनता के नुमाइंदों को समझना पड़ेगा कि देश की आजादी का रास्ता गरीब दलित और आदिवासी लोगों की माली व सामाजिक आजादी से हो कर जाता है. उन की आजादी के बिना इस आजादी का उत्सव अधूरा है.